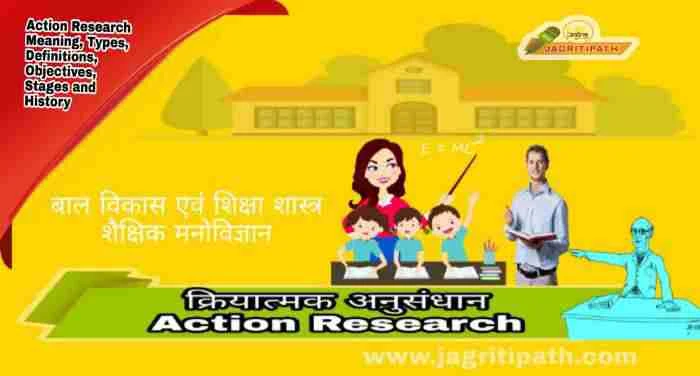 |
| kriyatmk-anusandhan Action Research Meaning, Types, Definitions, Objectives, Stages and History |
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें।स्टीफन एम. कोरे
क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना है। अनुसंधान एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है।
इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक स्वयं ही होते हैं। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान में संपादित करने में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अनुसंधान के अंतर्गत तत्कालीन प्रयोग पर अधिक बल देते हैं।
ये भी पढ़ें 👇
क्रियात्मक अनुसंधान के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही स्वयं शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक होते हैं। वीवी कामत ने अपने एक लेख में (कैन ए टीचर डू रिसर्च टीचिंग, 1975) भारत में अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है। भिन्न-भिन्न भाषाओं में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का शब्द भंडार, भारत में पब्लिक स्कूल, भाषा सीखने में भूलें, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की ऐच्छिक क्रियाएं। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की लंबाई, भार तथा अन्य शारीरिक लक्षण, भूगोल एवं इतिहास की अध्यापन पद्धतियां शामिल हैं।
क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार
|
|
-क्रियात्मक
अनुसंधान के प्रकार
|
1.क्रियात्मक अनुसंधान- अनुसंधानकर्ता – अध्यापक / निरीक्षक
2.मौलिक अनुसंधान- अनुसंधानकर्ता विद्यार्थी
क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषाएँ
|
|
-क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषाएँ
|
अर्थ - विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना।
उदाहरणार्थ : क्रियात्मक अनुसंधान से निरीक्षक अपने प्रशासन में प्रबन्धक विद्यालय की व्यवस्था में प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के संचालन में और शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकते हैं।
क्रि.अनुसंधान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं
1. मेक ग्रेथटे के अनुसार, "क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है।"
2.स्टीफन एम. कोरे के अनुसार, “शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान
है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें।"
3. Research education के अनुसार, "क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है, जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिये करता है।"
4. गुड़ के अनुसार, "क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यो की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है।"
5. मौले के अनुसार, "शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने वाली
समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समाधान चाहती है। मौके पर किये जाने वाले ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है, शिक्षा में साधारणतः क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से प्रसिद्ध है।"
6.रेडमेन एवं मोरी ने अनुसंधान को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है "नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है।"
क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास और प्रयोग
|
|
-क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास और प्रयोग
|
क्रियात्मक अनुसंधान वर्तमान जनतांत्रिक युग की देन है। इसे प्रतिपादित करने का श्रेय अमरीका को है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरीका में कोलियार द्वारा किया गया था।
इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेविन ने 1964 में मानव-संबंधों को बेहतर करने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग की सिफारिश की।
अमेरीका के राइटस्टोन ने 'पाठ्यक्रम ब्यूरो' के कार्यों के विवरण में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार टूबा, ब्रैडी और रॉबिन्सन ने समस्या समाधान के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रमुखता प्रदान की।
शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को स्थाई रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय अमेरीका के कोलंबिया विश्वविद्यालय स्टीफेन एम. कोरे को है जिन्होनें 1953 में यह कदम उठाया। 1953 में कोरे की पुस्तक विद्यालय की कार्यपद्धति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक : अनुसंधान' का प्रकाशन हुआ जिसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान को लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ी।
भारत में सर्वप्रथम कामता प्रसाद पांडे ने 1965 में शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान नाम की पुस्तक की रचना की थी उन्होंने बताया कि," शिक्षा संस्थाओं और शैक्षणिक अनुसंधान कर्ताओं के बीच एक ऐसी खाई सी बन गई है जिसे पाटना प्रजातंत्र की रक्षा हेतु नितांत आवश्यक बन गया है।
क्रियात्मक अनुसन्धान के उद्देश्य
|
|
-क्रियात्मक अनुसन्धान के उद्देश्य
|
(1) विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करना।
(2) छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातन्त्र के वास्तविक गुणों का
विकास करना।
(3) विद्यालय के कार्य-कर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य,
प्रबन्धक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास
करना।
(4) विद्यालय के कार्य-कर्ताओं में कार्य कौशल का विकास
करना।
(5) शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबन्धकों को विद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिये सुझाव देना। (6) विद्यालय की परम्परागत रूढ़िवादिता तथा यान्त्रिक
वातावरण को समाप्त करना।
(7) विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशली बनाना।
(8) छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊँचा उठाना।
क्रियात्मक अनुसन्धान का क्षेत्र
|
|
-क्रियात्मक अनुसन्धान का क्षेत्र
|
क्रियात्मक अनुसन्धान को विद्यालय की कार्य प्रणाली के अधोलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है
(i) कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाना है। (ii) शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये इसका
प्रयोग करते हैं।
(iii) छात्रों की अभिरूचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में
वृद्धि के लिये इसे प्रयुक्त करते हैं।
(iv) शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिये जाने वाले गृह
कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिये इसे
प्रयोग करते हैं।
(v) छात्रों की अनुसन्धान सम्बन्धी समस्याओं के समाधान
के लिये इस प्रयुक्त करते हैं।
(vi) भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वाचन की
समस्याओं के लिये तथा भाषाई शुद्धि के लिए भी क्रियात्मक -अनुसन्धान को प्रयुक्त किया जाता है।
(vii) छात्रों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय विलम्ब से आने
की समस्याओं के समाधान में इसे प्रयोग करते हैं।
(viii) छात्रों एवं शिक्षक सम्बन्धी समस्याओं तथा छात्रों में
परस्पर आदान-प्रदान की समस्याओं के लिये प्रयुक्त
करते हैं।
(ix) परीक्षा में छात्रों के नकल करने की समस्याओं के
समाधान में प्रयोग करते हैं।
(x) विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग करते हैं।
क्रियात्मक अनुसंधान के चरण/सोपान
|
|
-क्रियात्मक अनुसंधान के चरण/सोपान
|
1.समस्या का चयन
2.उपकल्पना का निर्माण
3.तथ्य संग्रहण की विधियाँ
4.तथ्यों का संकलन
5.तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण
6.तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष
7.सत्यापन
8.परिणामों की सूचना
एण्डरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के निम्न सात चरण बताये हैं
1. पहला सोपान : समस्या का ज्ञान : क्रिया-अनुसंधान
का पहला सोपान है।विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्या को भली-भाँति समझना। यह तभी सम्भव है,
जब विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक,प्रधानाचार्य आदि उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा करके ही वे
वास्तविक समस्या को समझकर अपने कार्य में आगे सुधार करना चाहते हैं।
2. दूसरा सोपान : कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचारविमर्श : क्रिया-अनुसंधान का दूसरा सोपान है–समस्या का भली-भांति समझने के बाद इस बात पर विचार करना कि उसके कारण क्या हैं और उसका समाधान करने के लिए
हमें कौन-से कार्य करने हैं। शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबन्धक आदि इन कार्यों के सम्बन्ध में अपने-अपने प्रस्ताव या सुझाव देते हैं। उसके बाद वे अपने विश्वासों, सामाजिक मूल्यों, विद्यालयों के उद्देश्यों आदि को ध्यान में रखकर उन पर विचार-विमर्श करते हैं।
3. तीसरा सोपान : योजना का चयन व उपकल्पना का
निर्माण : क्रियात्मक-अनुसन्धान का तीसरा सोपान है।विचार-विमर्श के फलस्वरूप समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण करना। इसके लिए विचार-विमर्श करने वाले सब व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। उपकल्पना में तीन बातों का सविस्तार वर्णन किया जाता है—
(1)समस्या का समाधान करने के लिए अपनाई जाने वाली योजना,
(2) योजना का परीक्षण,
(3) योजना द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य।
4. चौथा सोपान : तथ्य संग्रह करने की विधियो का
निर्माण : क्रिया-अनुसंधान का चौथा सोपान है योजना को कार्यान्वित करने के बाद तथ्यों या प्रमाणों का संग्रह करने की विधियाँ निश्चित करना—इन विधियों की सहायता से जो तथ्य संग्रह किये जाते हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है।
5. पाँचवाँ सोपान : योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों
का संकलन :क्रिया अनुसंधान का पाँचवाँ सोपान है. निश्चित की गई योजना को कार्यान्वित करना और उसकी सफलता या असफलता के सम्बन्ध में प्रमाणों या तथ्यों का संकलन करना योजना से सम्बन्धित सभी व्यक्ति चौथे सोपान में निश्चित की गई विधियों की सहायता से तथ्यों का संग्रह करते हैं। वे समय समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करते हैं। इसके आधार पर वे योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं।
6. छठा सोपान : तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष : क्रियात्मक अनुसंधान का छठा सोपान है,योजना की समाप्ति के बाद संग्रह किए हुए तथ्यों या प्रमाणों से निष्कर्ष निकालना।
7. सातवाँ सोपान : दूसरे व्यक्तियों को परिणामों की सूचना :क्रिया-अनुसंधान का सातवाँ और अन्तिम सोपान है
दूसरे व्यक्तियों को योजना के परिणामों की सूचना देना।
क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ
|
|
-क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ
|
1. इससे शिक्षक अपनी कक्षा के वातारण में
अपनी कार्यप्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है।
2. शिक्षक शोध के पदों से परिचित होता है।
3. शिक्षकों में वैज्ञानिक-प्रवृत्ति, शोध कार्य के लिए जाग्रत
होती है।
4. इसके द्वारा विद्यालय के प्रशासन में सुधार तथा परिवर्तन
लाया जाता है।
5. यह विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों की विभिन्न दैनिक
समस्यओं का व्यावहारिक एवं तथ्यपूर्ण समाधान करता है। 6. यह विद्यालय को आधुनिक तथा समयानुकूल बनाने
का प्रयास करता है।
7. इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष व्यवहारिक रूप से काफी सफल होते हैं।
ये भी पढ़ें |
बुद्धि: अर्थ,परिभाषा,प्रकार एवं सिद्धांत तथा संवेगात्मक बुद्धि ⇦Click here अधिगम अर्थ,परिभाषा,प्रकार एवं गेने की अधिगम सोपानिकी अभिवृद्धि एवं विकास , विकास की अवस्थाए,शैश्वास्था-बाल्यावस्था-किशोरावस्था |
OUTSTANDING SIR THANKS A LOT
ReplyDeleteShiksha Mein kriyatmak Anusandhan karykartaon dwara Kiya jane wala Anusandhan Hai Taki vah Apne Karya Mein Sudhar kar Saken Stephen M Kore
ReplyDeleteGood post
ReplyDeleteVery nice
ReplyDeleteबहुत ही उपयोगी पोस्ट है मेने भी यही से अपना कॉपी त्यार किया है
ReplyDeleteधन्यवाद
DeleteNice information
ReplyDeleteGood
ReplyDelete