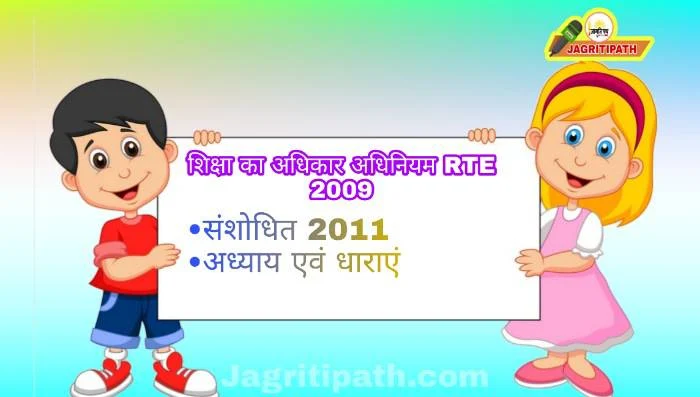 |
| Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act RTE 2009 |
भारत में शिक्षा का मुद्दा हमेंशा चर्चित और सुर्खियों में रहा तथा समय समय पर शिक्षा के बारे कई मांगे उठती रही। आजादी के बाद भी भारत में अशिक्षा और गरीबी दोनों प्रमुख समस्याएं रही । इसलिए भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का अनिवार्य करना महती आवश्यकता थी। विश्व के काफी देशों ने शिक्षा को अधिकार तथा अनिवार्य का रूप दे दिया था। इसलिए भारत में यह जरूरी हो गया था कि अशिक्षा को देखते हुए 6-14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना बेहद जरूरी हो गया था। इसके अलावा भारत में शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण यह भी जरूरी था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर प्रत्येक बालक-बालिका तक शिक्षा पहुंचे। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए भारत में शिक्षा का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। इसके बाद में भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और शत-प्रतिशत की पहुंच पूर्ण नहीं हो पाई है। इसलिए इस आरटीई का विस्तार करने की भी मांग उठ रही है।
6-14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया जिसे शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के रूप में राज्य सभा द्वारा 20 जुलाई, 2009 को पारित किया गया तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त, 2009 को 'द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कंपलसरी एजुकेशन बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21-ए के अन्तर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया - जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भारत 'शिक्षा' को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वाँ देश है। राजस्थान राज्य में धारा-38 का लाभ उठाते हुए वर्ष-2011 में 29 मार्च को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में लागू किया गया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-RTE 2009 मे 7 अध्याय और
38 धाराएँ है प्रत्येक अध्याय मे निम्न धाराएं हैं तथा 38 धाराओं का विस्तृत रूप इस
प्रकार हैं।
अध्याय-1-प्रारम्भिक
धारा-1,2
अध्याय-2-निशुल्क अनिवार्य
शिक्षा
धारा-3,4,5,
अध्याय-3-माता-पिता,सरकार
के कर्तव्य
धारा-6,7,8,9,10,11
अध्याय-4-स्कूल एवं शिक्षक
के उतरदायित्व
धारा-12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25,27,28
अध्याय-5-प्रारम्भिक पाठ्यक्रम
धारा-29,30
अध्याय-6-बालकों के अधिकारों
का संरक्षण
धारा-31 32 33 34
अध्याय-7-विविध
धारा-35 36 37 38
RTE ACT 2009 सभी 38 धाराएं
|
धारा -1- संक्षिप्त नाम -इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम
"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम
2009" है। - यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर
राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रैल, 2010
से
प्रभावी रूप से लागू होगा। -अनुच्छेद 29 व 30 के उपबंधो के अध्यधीन इस
अधिनियम के प्रावधान है। - मदरसों, वैदिक पाठशालाओं व धार्मिक
प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों व संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। |
|
धारा- 2 -इस धारा में (क से य) तक उपधाराएँ है। (क) 'समुचित सरकार'- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व संघ राज्य सरकार
को शामिल किया जाता है। (ख) 'प्रति व्यक्ति फीस' से, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस
से भिन्न किसी प्रकार संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है। (ग) 'बालक' 6 वर्ष से 14 वर्ष का कोई बालक या बालिका
से है। (घ) 'असुविधाग्रस्त समूह'- एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. अनाथ, HIV व कैंसर से प्रभावित माता
पिता का बालक, विधवा के बालक व निशक्त बालक या समुचित सरकार द्वारा घोषित
तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक भाषा व लिंग के आधार पर घोषित बालक। (राजस्थान नियमावली 28 मार्च 2016 के अनुसार) (ड) 'दुर्बल वर्ग'- समुचित सरकार द्वारा घोषित
ऐसे बालक जिनके माता-पिता या संरक्षक की आय न्यूनतम सीमा से कम हो अर्थात 2.50 लाख से कम वार्षिक आयद (2015-16) तक हो। (सत्र 2016-17 से राज्य सरकार 1 लाख तक कर दी है।) (च) 'प्रारम्भिक शिक्षा' पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक
की शिक्षा से है। (द) “विद्यालय'- कक्षा 1 से 8 तक के चार प्रकार के होते हैं
1. नीजि, 2. सरकारी, 3. अनुदानित, 4. विशेष श्रेणी विद्यालय जैसे केन्द्रीय स्कूल, नवोदय स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (य) 'राज्य बालक अधिकार संरक्षण
आयोग' बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा-17 के अधीन गठित राज्य बालक
अधिकार संरक्षण आयोग से है। |
|
धारा-3-निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
का बालक का अधिकार- नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अधिकार
है। बालक अपने नजदीक के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक शिक्षा
ग्रहण करने तक का अधिकार रखेगा। बालक किसी प्रकार की फीस या प्रभार या व्यय का
संदाय करने का दायी नहीं होगा। धारा- 4-प्रवेश न दिए गए बालकों या
जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबन्ध- जिस
बालक ने प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है उसे उसकी आयु के अनुसार कक्षा में
प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात् भी
प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क शिक्षा का हकदार होगा। |
|
धारा- 5-अन्य विद्यालय में स्थानांतरण
का अधिकार- यदि किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं
है तो T.C. मांगने पर तुरन्त जारी कि जायेगी। टी.सी. नहीं देने पर
संस्था प्रधान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। |
|
धारा- 6-समुचित सरकार और स्थानीय
प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्त्तव्य- इस अधिनियम के उपबन्धों को
लागू करने के लिए सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर
आस-पास के क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित करेगी। |
|
धारा- 7-वित्तीय और अन्य
उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना- केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में व्यय का
हिस्सा तय करना। समुचित सरकार इसे लागू करने हेतु धन उपलब्ध कराये। केन्द्रीय
सरकार धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से
राष्ट्रीय पाठ्याचार के ढांचागत कार्य को विकसित करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए
मानकों को विकसित और लागू करेगी तथा नवीनीकरण, अनुसंधान नियोजन और क्षमता
निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध
करवायेगी। |
|
धारा- 8-समुचित सरकार के कर्त्तव्य-
प्रत्येक बालक (6-14) को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी
तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल
वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो तथा किसी
आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने का निवारण न हो, प्राथमिक शिक्षा के लिए
पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को समय से विहित करना सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक बालक
द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा
पूर्ण करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगी। |
|
धारा- 9-स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य-
(क) प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। (ख)
धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को
सुनिश्चित करेगा। (ग) यह सुनि करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त
समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने का निवारण न हो, (घ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु
के बालकों के ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख रखेगा। (ड.) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक
द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे
पूरा करने को सुनिश्चित करेगा और मानीटर करेगा। (च) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत
विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारिवद और सीखने की सामग्री भी है, उपलब्ध कराएगा। (छ) धारा 4
में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण
सुविधा उपलब्ध कराएगा। (ज) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और
मापमान के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करेगा। (झ) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को समय से
विहित करने को सुनिश्चित करेगा। (ण) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण
सुविधा उपलब्ध कराएगा। (ट) प्रवासी कुटुंबों के बालकों के
प्रवेश को सुनिश्चित करेगा। (ठ) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्य को मानीटर करेगा, और (ड) अकादमिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा। स्थानीय प्राधिकारी का यह
कर्तव्य है कि शैक्षिक कलैण्डर, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रवेश आदि की
व्यवस्था करना। |
|
धारा-10-माता-पिता और
संरक्षक का कर्त्तव्य- प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि
वह आस-पास के विद्यालय में अपने बच्चों का प्रवेश कराए। |
|
धारा-11-समुचित सरकार का विद्यालय- पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना-
प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से ऊपर के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों
के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से
समुचित सरकार ऐसे बालकों के लिए नि:शुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के
लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी। |
|
धारा-12- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। 12 (1)
ग के
अनुसार दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को नीजि विद्यालयों के पहली
कक्षा/प्रारम्भिक कक्षा के कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जायेगा। 12 (2)
के
अनुसार इनकी फीस का पुर्नभरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। यदि विद्यालय
पूर्व शिक्षा की व्यवस्था किसी स्कूल में है तो वहां पर भी यह नियम लागू होगा |
|
धारा-13-प्रवेश पर कोई
फीस नहीं तथा प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाये। उल्लघन करने पर प्रवेश शुल्क के 10 गुना तथा प्रवेश परीक्षा पर 25000 रु. जुर्माना होगा। |
|
धारा-14-प्रवेश के लिए
आयु का सबूत न होने पर भी विद्यालय में बालक को प्रवेश से इन्कार नहीं किया जा
सकता। |
|
धारा-15-प्रवेश से इन्कार
न किया जाना- प्रवेश की निर्धारित दिनांक के बाद भी अगर कोई बालक विद्यालय में
प्रवेश लेना चाहे तो विद्यालय इंकार नहीं कर सकता। |
|
धारा-16-रोकने और
निष्कासन का प्रतिषेध रोकने से तात्पर्य - कक्षा 8 तक किसी बालक को फेल
नहीं किया जाएगा। निष्कासन से तात्पर्य - विद्यालय से
प्राथमिक शिक्षा के पूरा किए जाने तक बालक का विद्यालय से नाम प्रथक नहीं किया |
|
धारा-17-बालक के शारीरिक
दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध तथा अपमानजनक शब्दों से सम्बोधित नहीं करें। |
|
धारा-18- मान्यता प्रमाण
पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। ऐसा करने पर एक
लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। |
|
धारा-19- विद्यालय के मान एवं मानक- विद्यालय प्रारम्भ से तीन वर्ष की
अवधि में पूरा किया जाये। नये और पुराने स्कूलों को ध रा-18 के अन्तर्गत तय मापदण्ड पूरे ना करने पर मान्यता नहीं दी जायेगी।
बिना मान्यता के विद्यालय खोलने पर एक लाख रूपये का जुर्माना अदा करना होगा। |
|
धारा-20-अनुसूची में
संशोधन करने की शक्ति- 'केन्द्र सरकार' द्वारा एक लिखित
अधिसूचना द्वारा संशोधन कर किसी मान या मानक को अनुसूचि में जोड़ा जा सकता है या
हटाया जा सकेगा। |
|
धारा-21 विद्यालय
प्रबंधन समिति - विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय
में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों
के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलाकर
एक 16 सदस्यों की विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करेगा। इस समिति
में कम से कम तीन-चौथाई (75%)
सदस्य माता या संरक्षक होगें। इस
समिति में 50% सदस्य महिलाएं होगी। |
|
धारा- 22-विद्यालय विकास
योजना- विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। |
|
धारा- 23-शिक्षकों की
नियुक्ति के लिए योग्यताएं/अर्हताएं और सेवा शर्ते। धारा- 24-शिक्षकों
के कर्त्तव्य और
शिकायतों को दूर करना। |
|
धारा-25-छात्र शिक्षक
अनुपात- यह तीन वर्ष के अंदर लागू होना चाहिए। |
|
धारा- 26-शिक्षकों की
रिक्तियों को भरा जाना अर्थात् 10%
से
अधिक पद रिक्त नहीं रखें जायें। |
|
धारा- 27-गैर-शैक्षिक
प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध केवल तीन कार्यों
को छोड़कर (i) 10 वर्षीय जनगणना, (ii) आपदा राहत, (iii) चुनाव कार्य तथा इनके अलावा अन्य
गैर-शैक्षिक कार्य नहीं करवाये जाएगे। |
|
धारा- 28-शिक्षक द्वारा
प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान। |
|
धारा-29-1. प्रारंभिक
शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा लिखित सूचना
द्वारा तय किए जाने वाले शैक्षिक अधिकारी या संस्था के निर्देशन में तैयार होगा।
2. सरकार
द्वारा तय शैक्षिक अधिकारी या संस्था पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार
करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे कि(क) पाठ्यक्रम और मूल्यांकन
प्रक्रिया संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप हो। '(ख) बालक का सर्वांगीण विकास करें। (ग)
बालक में ज्ञान का, अन्तःशक्ति
और योग्यता का निर्माण हो। (घ) बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता के विकास का
अधिकतम अवसर हो। (ड) सीखने सिखाने की प्रक्रिया बालकों के अनुरूप गतिविधि आधारित
हो और खोजने की प्रवृति बढ़ाने वाली हो। (च) शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके
बच्चों की मातृभाषा के अनुरूप हो। (छ) स्कूल में भयमुक्त वातावरण हो ताकि बच्चे
स्वयं सोच-विचार कर निर्णय ले सकें। (ज) बच्चों के सीखने और समझाने का व्यापक
एवं सतत् आकलन (सी.सी.ई.) शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही हो। |
|
धारा -30-1. प्रारम्भिक
शिक्षा यानि कक्षा 8 पूरी करने
तक किसी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं होगा। 2. बच्चों को
कक्षा 8 तक की
शिक्षा पूरी करने का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जो कि सरकार द्वारा तय किया जाएगा। |
|
धारा -31- बालकों
के अधिकार का संरक्षण बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना- राष्ट्रीय बालक
अधिकार संरक्षण आयोग 2005 या राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के
द्वारा बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। |
|
धारा -32-बालक की शिकायतों को तीन माह के अन्दर
दूर करना। तथा सबसे पहले शिकायत लिखित रूप में स्थानीय अधिकारी उसके बाद बाल
अधिकार संरक्षण आयोग में की जायेगी। |
|
धारा -33-केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद का गठन करना। |
|
धारा -34-राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना |
|
धारा -35-निर्देश जारी करने की शक्ति- केन्द्रीय सरकार (भारत सरकार)
राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को दिर्नेश जारी करती है। |
|
धारा -36 दण्डनीय अपराधों की कार्यवाही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी
से पूर्व अनुमति लेना जैसे धारा-13,
धारा-18 तथा
धारा-19 |
|
धारा -37- केन्द्र सरकार व राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबन्धन समिति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किसी
निर्णय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। |
|
धारा -38- समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति
तथा राज्य सरकारें इसके क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचना जारी कर बना सकेगी
जैसे- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 |
बहुत ही बढ़िया पोस्ट की हुई है आरटीई 2009 के बारे में जानकारी है
ReplyDelete👌👌👌
ReplyDelete❣️
DeleteGreat post very useful 👌👍
ReplyDelete