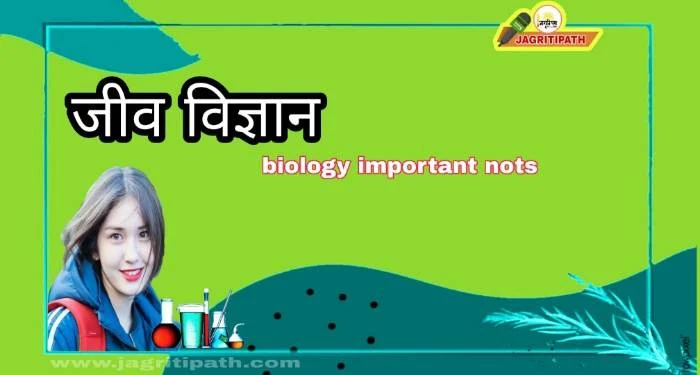 | |
|
Biology शब्द का सर्वप्रथण प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन् 1801 में किया था। जीव विज्ञान को दो भागों में बाँटा गया है: (i) जन्तु विज्ञान (Zoology) (ii) वनस्पति विज्ञान (Botany)
सजीवता के लक्षण
सजीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं, जो उन्हें निर्जीवों से पृथक करते हैं। ये लक्षण निम्न हैं आकृति एवं मापछाति, कोशिकीय संरचना उपापचयह श्वसना वृद्धि एवंविकास, उत्सर्जन ठत्तेजनशीलताअनुकूलन जनन जीवन चक्र
कोशिका (Cell)
कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। • कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ई. में अंग्रेज़ वैज्ञानिक राबर्ट हुक ने कार्क की पतली काट में की। एन्टोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने पादप.कोशिका में हरित लवक की खोज की। पुरकिन्जे ने कोशिका में जैली जैसे गाढ़े द्रव्य को 'प्रोटोप्लाज्म' नाम दिया।राबर्ट ब्राउन ने सन् 1831 में कोशिका में केन्द्रक की खोज की।
श्वान और श्लाइडेन ने सन् 1838-39 में कोशिका सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। जन्तुओं में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अमीबा, पेरामीशियम, युग्लीना, प्लाज्मोडियम का शरीर एक हमारे शरीर में अनुमानतः एक हजार खरब कोशिकाएं पायी जाती है। वे कोशिकाएँ जिनमें सुस्पष्ट केन्द्रक व केन्द्रक झिल्ली का अभाव होता है, प्रौकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं । जैसेजीवाणु कोशिका। वे कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केन्द्रक व केन्द्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जन्तु कोशिका में जीवद्रव्य एक महीन झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह प्रोटीन-वसा-प्रोटीन की बनी होती है।
पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलूलोज की परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। . कोशिका झिल्ली से परिबद्ध समस्त जैली जैसा गाढ़ा पदार्थ जीव द्रव्य (Protoplasm) कहलाता है। कोशिका झिल्ली से केन्द्रक झिल्ली के मध्य स्थित समस्त जीवद्रव्य
कोशिका द्रव्य (Cytoplasm) कहलाता है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकान्ड्रिया की खोज कोलीकर ने की थी तथा इसे 'माइटोकान्ड्रिया' नाम बेन्डा ने दिया था।
गॉल्जीकाय की खोज केमिलो गॉल्जी ने की थी। अन्त:प्रदव्यी जालिका की खोज केथ पोर्टर ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी-ड्यूबे ने की थी।
लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ (Suicidal bags) भी कहा जाता है। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इन्हें 'कोशिका इंजन' भी कहा जाता है 'Cytoplasm' शब्द स्ट्रासबर्गर ने दिया था। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है-(i) असूत्री (ii) समसूत्री (iii) अर्ध सूत्री। असूत्री विभाजन,की खोज रेमाक ने की थी। यह विभाजन अनेक जीवाणुओं, शैवाल व कवकों में पाया जाता है। 'Mitosis' शब्द सन् 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया। समसूत्री विभाजन 'Mitosis' में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही रहती है। हमारे शरीर की वृद्धि कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन ही होता है। जिससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है। अर्द्धसूत्री विभाजन (Meiosis) में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती है। यह विभाजन हमारी जनन ग्रन्थियों की जनन कोशिकाओं में होता है। जिससे नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अर्द्धसूत्री विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल DNA (डी-ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल), RNA (राइबो न्यूक्लिक अम्ल) पाये जाते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने DNA मॉडल प्रस्तुत किया एवं उन्होंने बताया की DNA एक द्वि कुण्डलित सीढ़ीनुमा संरचना में होता है। 3.जैव जगत में संगठन के स्तरः जैव जगत में संगठन के निम्न स्तर है: परमाणु → अणु→ यौगिक → कोशिका अंग → अंग तंत्र → उच्च स्तर है
जीव→ जनसंख्या जैव समुदाय -→ पारिस्थितिकी तंत्र
→ जैव मण्डल।
पारिस्थितिकी तंत्र
जैव समुदाय का उसके पर्यावरण के साथ सम्बन्धों से बनने वाला तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसे-तालाब, समुद्र, नदी का पारिस्थितिकी तंत्र। जैव मण्डल तीनों मण्डलों (जल, स्थल, वायु मण्डल) में कुल 21 किमी. में विस्तारित है। जो वायुमण्डल में 9.6 किमी. ऊँचाई तक स्थल मण्डल व 11.2 किमी. गहराई तक जल मण्डल तक फैला हुआ है। जैव मण्डल के घटक: जैव मण्डल के घटकों को दो भागों में बाँटा गया है:
भौतिक या अजैविक घटक: वायुमण्डलीय गैसें, प्रकाश, तापक्रम, घर्षण, मृदा, आर्द्रता, स्थलाकृति, आदि।
जैविक घटक-विभिन्न पादप, जन्तु, सूक्ष्मजीव एवं मनुष्य।
वायुमण्डलीय जल (जलवाष्प) का वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर आना तथा पुन: वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण द्वारा वायुमण्डल में पहुँचने की चक्रीय घटना जल-चक्र कहलाती है।
मृदा को परतीय संरचना को मृदा परिच्छेदिका (Soil Profile) कहते हैं। जिसने ऊपर से नीचे क्रमशः तीन संस्तर A.(शीर्षमृदा),B. ( अधोमृदा), C. (पैतृक पदार्थ/चट्टान) होते हैं।
मृदा का संगठन चार घटकों खनिज (45%), कार्बनिक पदार्थ (5%), मृदा जल (25%), मृदा वायु (25%) द्वारा होता है। वायुमण्डल ने CO2 की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसे पौध घर प्रभाव (Green house effect) कहते हैं।
जैव समुदाय के पोषक स्तरः
समस्त जैव मण्डल के लिए ऊर्जा का एक मात्र स्रोत सूर्य ही है। सभी जीव सौर ऊर्जा का ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उपभोग करते हैं।• उत्पादकः
वे सजीव जो सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष उपभोग कर अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता:
उत्पादकों का उपभोग करने वाले जन्तु प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाते हैं।
द्वितीयक उपभोक्ताः
प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले जन्तु, द्वितीयक उपभोक्ता या माँसाहारी कहलाते हैं।
तृतीयक उपभोक्ताः
द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले जन्तु,
तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी कहलाते हैं।
• अपघटक जीवः वे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन मृत कार्बनिक
पदार्थों से प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक कहलाते हैं।
• खाद्य श्रृंखला:
भोजन के आधार पर बनी जीवों की क्रमिक
श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
खाद्य जाल: खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में मिलने से बने जाल को खाद्य जाल (Food web) कहते हैं।
जीव की उत्पत्तिः
इस सदर्भ में प्रतिपादित मुख्य सिद्धान्त निम्न है: (i) स्वतः जननः सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से स्वत: ही हो जाती है। प्रतिपादक: अरस्तू, ल्युक्रेशियस, वॉन हेल्मान्ट। (ii) कॉस्मिक पैन्स्पर्मियाः जीव पृथ्वी पर उत्पन्न न होकर अन्य किसी आकाशीय पिण्ड से आया है। प्रतिपादक: कैल्विन, अरेनियस। (ii) संयोग सृजन: जीव की उत्पत्ति असाधारण संयोग के द्वारा हुई है। प्रतिपादक: हैरोडोट्स, एम्पिडोकिलरा। हिन्दू दर्शन के अनुसार जीव की उत्पत्ति पंचमहाभूतों से हुई है। (iv) जीवात् जीवोत्पत्तिः जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है।
प्रतिपादक: लुई पाश्चर (v) रासायनिक विकास: जीव की उत्पत्ति विभिन्न यौगिकों के रासायनिक संश्लेषण से समुद्र में हुई है। प्रतिपादक: ए. आई.ओपरिन (1982) इस सिद्धान्त की पुष्टि स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा की है।
जैव विकास के सिद्धान्तः
(i) उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धान्तः
इस सिद्धान्त के अनुसार उपयोगी अंगों में वृद्धि तथा अनुपयोगी अंगों में ह्रास होता है। कालान्तर में इस प्रकार एक नई जाति बन जाती है। पतिपादक:लैमार्क
(ii) प्राकृतिक वरण का सिद्धान्तः
इस सिद्धान्त के अनुसार
प्रकृति बहुसंख्यक जीवों में से योग्यतम का चुनाव करती हैं। प्रकृति के इस क्रमिक चुनाव से कालान्तर में एक नवीन जाति की उत्पत्ति हो जाती है। इस सिद्धान्त के चार प्रमुख चरण है: संतानोत्पत्ति की अधिक दर, जीवन संघर्ष, प्राकृतिक वरण, नई जातियों की उत्पत्ति । प्रतिपादक: चार्ल्स डार्विन (Book :Origin of Species by Natural Selection)
(iii) उत्परिवर्तनवादः
आनुवंशिक संरचना में अचानक परिवर्तनसे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। प्रतिपादक ह्यगो डी ब्रीज।
(iv) नव डार्विनवादः
आधुनिक खोजों के अनुसार डार्विनवादका संशोधित एवं परिष्कृत रूप नव डार्विनवाद कहलाता है।
जैव विकास के प्रमाण:
जीवाश्म प्रमाण, शरीर रचना प्रमाण (समजात, समवृत्ति अंग), भ्रूणीय प्रमाण, अवशेषी अंग, संयोजक कड़ियाँ, भौगोलिक वितरण, शरीर क्रियात्मक प्रमाण, वर्गीकी प्रमाण।जन्तु जगत का वर्गीकरणः
पृष्ठ रज्जू की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बाँटा गया है :(i) अपृष्ठ वंशी (नॉनकॉर्डेटा), (ii) पृष्ठ वंशी (कॉर्डेटा)। अपृष्ठी वंशी: इसे निम्न संघों में वर्गीकृत किया गया है:
प्रोटोजोआ, पारिफेरा, सीलेन्टेटा, एस्केहैल्मिन्थीज, प्लेटिकैल्मिथीज,आथ्रोपोडा, मोलस्का, इकॉइनोडर्मेटा।
पृष्ठी वंशी: इसे निम्न संघों में वर्गीकृत किया गया है: पीसीज
(मछली वर्ग), एम्फीबिया (उभयचर वर्ग),रेप्टीलिया (सरीसृप वर्ग), एवीज (पक्षी वर्ग), मैमेलिया (स्तनधारी वर्ग)।
No comments:
Post a Comment