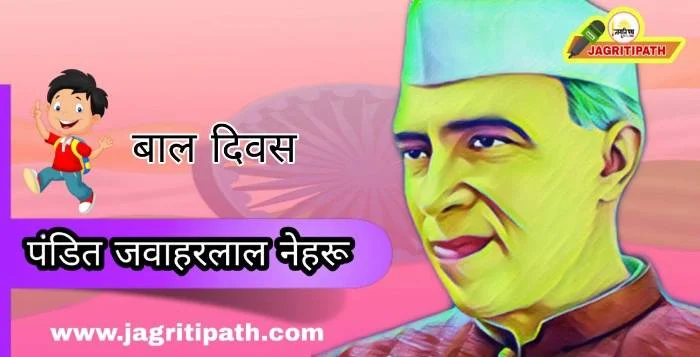 |
| November 14: Children's Day is celebrated as the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru |
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री,चाचा के नाम से प्रसिद्ध तथा बाल प्रिय नेहरू जिनकी जयंती पर भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि पंडित नेहरू के निधन से पहले देश में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था.
14 नवम्बर 2020 को भारत में दीपोत्सव के साथ साथ चाचा नेहरु की 131 वीं जयंती मनाई जा रही है। पंडित नेहरू भारत की विदेश नीति और राजनीति के सफर में गांधी के बाद पहले शख्स थे जिन्हें भारत सहित पूरे विश्व में सम्मान के साथ याद किया जाता है। नेहरू समाजवाद, मानवतावाद के प्रबल समर्थक के भारत में गरीबी खत्म करने तथा पिछड़े तबकों को ऊपर लाने के लिए उन्होंने पूंजीवाद के समर्थन की बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। आजादी की लड़ाई में भी नेहरू जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक भारत के निर्माण और विकास में नेहरू जी का आसीम योगदान है। इसलिए नेहरू की प्रतिभा के अनेक पक्ष अब इतिहास का अंग बन चुके हैं। किन्तु हम इस महान मुक्तिदाता के आदर्शों और नीतियों को तब तक नहीं समझ पायगे, जब तक हम उस दर्शन को न समझ लें, जो इन आदर्शों और नीतियों में अंतर्निहित था और यह न जान लें कि किस प्रकार इसने उनके विचारों के निर्माण में सहायता की।
जीवन परिचय, शिक्षा, सक्रियता और स्वाधीनता संग्राम में संघर्ष
जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) पिता मोतीलाल नेहरू और स्वरूपरानी के एकमात्र पुत्र थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था।
15 वर्ष की आयु में वे अध्ययन के लिए इंग्लैण्ड गए। 1905 में उन्हें इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में प्रविष्ट कराया गया तथा 1907 में उन्होंने ट्रिनीली कालेज, कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया जहां उन्होंने विज्ञान में आनर्स' की परीक्षा पास की। कैम्बिज की पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया और 1912 में वे 'इनर टेम्पल' से वकील बने। अपने छात्र जीवन में ही नेहरू भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते रहे। 1904 में जापान के हाथों रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र की पराजय ने नेहरू के हृदय में भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता के सपने भर दिए । राष्ट्रीय विचार उनके मानस में हिलोरें लेने लगे और यूरोप के कब्जे से भारत तथा एशिया की मुक्ति के लिए वे परेशान रहने लगे।
अपने शिक्षा काल में वे सिडनी वैब तथा बैट्रिरा वैब की फेबियन समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। यद्यपि वे स्वयं वैभव में पैदा हुए थे और उनके समक्ष जीवन यापन की समस्या कभी उत्पन्न नहीं हुई, पर उनका दृष्टिकोण ऐश-आराम के जीवन की उपज नहीं था, जो चारों ओर व्याप्त आंदोलन और ऊथल-पुथल से अलग हो। इस दृष्टिकोण का जन्म टकरावों और संघर्षों के बीच हुआ था। भारत में आकर उन्होंने वकालत करना प्रारम्भ किया जिसमें उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली और वे सार्वजनिक जीवन की दिशा में मुड़े। 1912 में वे बांकीपुर(बिहार) के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। वे गांधीजी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में संचालित "रंगभेदी विरोधी आन्दोलन" के विवरण से प्रभावित हुए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वे गांधीजी से मिले। 1918 में वे कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुने गए। रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला हत्याकाण्ड पर व्याप्त भारी असंतोष से नेहरू प्रभावित हुए। 1919 में नेहरू ने पहली बार गांवों में घूम-घूम कर भारत वर्ष के नंगे भूखे किसानों को देखा तथा उनके लिए सेवा कार्य करने का निश्चय किया।
इस प्रकार देश की राजनीतिक परिस्थिति में तीव्र उद्वेग आने के साथ हर चीज बदल गयी। प्रथम महायुद्ध और उसके दुष्परिणामों, तिलक और एनीबिसेन्ट के होमरूल आन्दोलन, जलियांवालाबाग हत्याकाण्ड तथा गांधीजी के नेतृत्व में व्यापक विरोध आन्दोलन- इन सबका जवाहरलाल के संवेदनशील मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यदि भूख, अज्ञान और गंदगी को मिटाया नहीं जाता तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।
नेहरू का राजनीतिक क्षितिज क्रमशः विस्तृत होने लगा। यूरोपीय देशों में उनके प्रवास, 1927 में सोवियत संघ की उनकी यात्रा, नये साम्राज्यवाद विरोधी उभार, पूंजीवाद के विश्व संकट और सोवियत संघ की प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता- इन सबके शक्तिशाली प्रभाव के कारण वह समाजवादी विचारों के निकट आए। वह अब प्रबल रूप से अनुभव करते थे कि पूंजीवाद की प्रगतिशील क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं और भविष्य की चुनौति का एकमात्र उत्तर समाजवाद है।
यूरोप में रहते समय, 1927 में उन्होंने औपनिवेशिक जनता की ब्रूसेल्स कांग्रेस में भाग लिया तथा रोमां रोला, एल्बर्ट आइस्टीन और सुंग चिंग लिंग जैसी विश्वविख्यात बुद्धिजीवी प्रतिभाओं के साथ मिल कर "साम्राज्यवाद के विरूद्ध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय लीग' की स्थापना की। भारत लौटने पर वह नयी शक्ति और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ साम्राज्यवाद-विरोधी कार्यवाहियों में जुट गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को नया रूप और नई अन्तर्वस्तु प्रदान की। वे कांग्रेस के युवा नेता
थे। उन्होंने कांग्रेस का लक्ष्य देश के लिए "औपनिवेशिक स्वराज्य' के बजाय “पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति" बना दिया तथा 1928 में 'इन्डिपेन्डेस लीग' स्थापित की। वे 'नेहरू-रिपोर्ट' में प्रस्तावित 'औपनिवेशिक स्वराज्य' के लक्ष्य से असहमत थे। 1928 में उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया और लाठी प्रहार सहे। 1929 में इतिहास-प्रसिद्ध लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के वे अध्यक्ष बने जिसमें देश के लिए "पूर्ण स्वाधीनता' के लक्ष्य की उद्घोषणा की गई।
भारतीय राजनीति में गांधी के अग्रगामी बने नेहरू
1930 तक जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था। और बाद के वर्षों में तो राष्ट्रीय नेतृत्व के क्षेत्र में उन्हें गांधीजी के ठीक बाद स्थान प्राप्त हो गया। उन्होंने गांधीजी के नेतृत्व में संचालित "सविनय अवज्ञा आन्दोलन' (1930-34) में सक्रिय भाग लिया। नेहरू ने 1936 में बिहार की भूकम्प पीड़ित जनता की भारी सेवा की। वे चार बार (1929, 1936, 1937 व 1946) कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा 9 वर्ष से भी अधिक काल तक वे जेल में रहे। अपने समाजवादी विचारों के आधार पर उनको 1938 में कांग्रेस की "राष्ट्रीय योजना समिति' की अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में वे चीन गए। 1942 में उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन" अथवा "अगस्त क्रांति" में सक्रिय भाग लिया। 1945 में उन्होंने वायसराय द्वारा आयोजित शिमला-सम्मेलन में भाग लिया तथा आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को छुड़वाने के लिए अदालती कार्य किया। 1948 में उनको मंत्रिमण्डलीय-आयोग (केबीनेट मिशन) के सुझावों के अनुसार बनायी गयी अन्तरिम सरकार में गवर्नर -जनरल की कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बनाया गया। भारत की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने ही नये भारत के लिए संविधान बनाने से संबंधित 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objective Resolution) 13 दिसम्बर 1946 को रखा। वर्तमान भारतीय संविधान बनाने के पीछे नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था। 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन की कीमत पर देश को स्वतंत्रता मिली तो जवाहरलाल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक (27 मई 1964) इसी पद पर बने रहे। महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल की मृत्यु के बाद वे ही कांग्रेस के एकछत्र सर्वोपरि नेता थे। उन्हीं के नेतृत्व में नये भारत का निर्माण हुआ। लगभग 17 वर्षों के अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक सबल आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को जमाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। नेहरू न केवल एक महान देशभक्त, कर्मठ राजनेता और शांतिदूत थे बल्कि बुद्धिमान और युगदृष्टा पुरूष थे, जिन्हें साहित्य, दर्शन व प्रकृति से भारी प्रेम था।
नेहरू जी की प्रमुख रचनाएं
नेहरू जी अनेक ग्रन्थों की रचना की, जिनमें निम्न रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं
विश्व इतिहास की झलक (Glimpses of World History). 1934, आत्मकथा (An Auto Biography), 1936, भारत की एकता (The Unity of India), 1947, भारत की खोज (The Discovery of Indi) उनकी अन्य कुछ रचनाएं है
लैटर्स फ्राम ए फादर टु हिज डॉटर, 1929; टुवर्डस फ्रीडम, 1941; उनके भाषणों को सम्पूर्ण रूप से बिफोर एण्ड आटर इण्डिपेन्डेन्सः जवाहरलाल नेहरूज़ स्पीचेज' (चार खण्ड) तथा सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू (आठ खण्ड) में प्रकाशित किया गया है।
मानवतावादी विचारक थे नेहरू
नेहरू एक राजनीतिज्ञ थे. लेकिन नैतिक आदर्शवाद में उनकी गहन आस्था जीवनभर बनी रही। पीड़ित और शोषित लोगों के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रीति और सहानुभूति थी । “एक मानव के रूप में उनके चिन्तन में सुकुमारता, भावना की अद्वितीय कोमलता और महान एवं उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण था।" वे मूलतः मानवतावादी हैं। उनकी विचारधारा का मूल केन्द्र “मानव' है। वे व्यक्ति को साध्य तथा शेष सभी को साधन मानते थे, चाहे वह राज्य हो, या राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीयता। उनकी दृष्टि में मानवतावाद आधुनिक युग का सर्वोत्तम आदर्श होना चाहिए था। "मैकियावलिय राजनीति", शोषण, अनाचार और अभाव को देखकर उनके हृदय में गहरी वेदना पहुँचती थी।
नेहरू मनुष्य के गौरव में विश्वास करते थे, इसलिए परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए भी, वे एक तानाशाह बन जाने के प्रलोभन से बचे रहे। वे लोकतांत्रिक समाजवादी बने रहे, मानवीय मूल्यों में उनकी आस्था कभी नहीं डगमगाई और साम्यवाद के हिंसक तथा अनैतिक साधनों के प्रति उन्हें कभी कोई आकर्षण नहीं रहा। जीवनभर उन्होंने अन्याय और शोषण से यथाशक्ति संघर्ष किया।
भारत के प्रथम सफल प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू
नेहरू ने पहले आजादी की लड़ाई का सफल नेतृत्व किया तथा फिर अपने प्रधानमंत्रित्व काल में स्वतंत्र भारत का हर क्षेत्र में कुशल मार्गदर्शन किया। 27 मई 1964 को उनके निधन के साथ ही भारत में एक युग की समाप्ति हुई, जिसे नेहरू-युग कहा जा सकता है। नेहरू ने राष्ट्र के भव्य प्रासाद को दृढ आधारशिला प्रदान की, संविधान के तन में जीव और जीवात्मा को प्रतिष्ठित किया, प्रारम्भिक 14 वर्षों में सविधान के सफल क्रियान्वयन के दौरान, संविधान की इमारत में जब-तब जो दरारें दिख पड़ी, नेहरू ने स्वयं अपने कर-कमलों से उनकी मरम्मत की। उन्होंने संविधान में जरूरी संशोधन प्रस्तुत करके संविधान निर्माताओं की वास्तविक भावनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में वे भारत की प्रगति. वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, लोकतांत्रिक-समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और स्वतंत्र विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए जूझते रहे। नेहरू एक सच्चे राष्ट्रवादी एवं अन्तर्राष्ट्रीयवादी थे। मानवमात्र के कल्याण की इच्छा रखने के नाते उन्होंने सदैव विश्व बन्धुत्व, सहयोग, शांतिपूर्ण - सहअस्तित्व, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता, असंलग्नता, निःशस्त्रीकरण तथा अणुशक्ति के शांतिपूर्ण रचनात्मक प्रयोग का समर्थन किया।
No comments:
Post a Comment